राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आर जी सी बी) एक उभरती हुई घटना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित, आर जी सी बी की शुरुआत 1990 में एक छोटे से धर्मार्थ समाज के रूप में हुई थी, जिसका नाम शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सी-डेस्ट) था। 1991 में, इसकी क्षमता को पहचानते हुए, सी-डेस्ट को केरल सरकार का "अनुदान-सहायता" संस्थान बनाया गया और इसका नाम बदलकर राजीव गांधी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (आरजीसी-डेस्ट) कर दिया गया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर देश का पहला संस्थान बन गया। 18 अप्रैल, 1994 को केरल सरकार ने संस्थान को एक व्यापक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में पुनर्गठित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और इस प्रकार राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया। संस्थान का प्रबंधन पहले केरल सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण समिति (एसटीईसी) और बाद में केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा किया जाता था। नए भवन की आधारशिला 18 नवंबर, 1995 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा रखी गई थी। ठीक सात साल बाद, 18 नवंबर, 2002 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने व्यापक केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। संस्थापक निदेशक डॉ. एम. रामचंद्र दास और उनके उत्तराधिकारी डॉ. आर.वी. थम्पन के मार्गदर्शन में, आर जी सी बी ने कद, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान उत्पादन में तेजी से वृद्धि की। अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि राज्य सरकार से आर जी सी बी को उपलब्ध संसाधन संस्थान की प्रगति की बराबरी नहीं कर सकते थे। केरल के राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी परिपक्वता और दूरदर्शिता का परिचय दिया, जिसमें तीन क्रमिक मुख्यमंत्रियों, श्री ई.के. नयनार, श्री ए.के. एंटनी और श्री ओमन चांडी ने आर जी सी बी को एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया। अब तक संस्थान ने चिकित्सा और पादप जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी खोजों और निष्कर्षों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त कर ली है।
28 फरवरी, 2006 को संसद में केंद्रीय बजट पेश करते समय माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने घोषणा की, "यदि कृषि एक प्राचीन भारतीय कौशल है, तो जैव प्रौद्योगिकी एक नया क्षेत्र है जिसे भारत जीतेगा। जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल को एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने का फैसला किया है।".
यह भारत में किसी भी शोध केंद्र को मिलने वाली सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आर जी सी बी ने केरल सरकार और लोगों के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उस पर रखे गए भरोसे, विश्वास और भरोसे को स्पष्ट रूप से पूरा किया है, जिसने लगभग एक दशक तक अनुसंधान अनुदान के माध्यम से केंद्र का लगातार समर्थन किया था। नियति के साथ हमारी लंबे समय से प्रतीक्षित मुलाकात 2 अगस्त, 2007 को एक वास्तविकता बन गई, जब माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 1 अप्रैल, 2007 से आर जी सी बी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, माननीय केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और महासागर विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने केरल सरकार को आर जी सी बी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के संस्थान के रूप में विकसित करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कैंसर अनुसंधान, उभरते वायरल संक्रमण और नैनो-बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक कार्यक्रमों सहित संस्थान के लिए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।
आर जी सी बी के एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पुनर्जन्म और इसके बाद के विकास ने इसके शोध और विकास कार्यक्रमों को फिर से परिभाषित करने की अनुमति दी है। हमारे शोध कार्यक्रम अब रोग जीवविज्ञान के केंद्रीय विषय पर जांच के समूहों के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं। इस ढांचे में मानव रोग, पशु रोग और पौधे रोग में बुनियादी और अनुप्रयुक्त कार्यक्रम शामिल हैं।
राष्ट्रीय संस्थान बनने के बाद के वर्षों में आर जी सी बी के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने जैव-नवप्रवर्तन केंद्र बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ मान्यता प्राप्त की। केरल राज्य सरकार ने शहर में आर जी सी बी को 20 एकड़ की प्रमुख भूमि हस्तांतरित करके बहुत ही उदारतापूर्वक जवाब दिया। जैव-नवप्रवर्तन केंद्र गहन और उन्नत स्तर के तकनीकी प्लेटफार्मों, बहु-विषयक कोर पर आधारित मध्यम और उच्च स्तर के नवाचार के लिए एक अद्वितीय ज्ञान केंद्र और केंद्र होगा जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा। इस परिसर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई इमारत की आधारशिला भारत सरकार की तत्कालीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जयपाल रेड्डी ने रखी थी।
आर जी सी बी वर्तमान में तीन परिसरों से कार्य करता है। केरल की राजधानी के केंद्र में जगथी में स्थित मुख्य परिसर वह जगह है जहाँ आर जी सी बी अपने अधिकांश खोज अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता है। परिसर रोग जीवविज्ञान अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है और मानव, पशु और पौधों की बीमारियों के सेलुलर और आणविक तंत्र में अभिनव अध्ययन करता है। जांच के तहत रोग क्षेत्रों की श्रेणी में कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस और हृदय रोग, तपेदिक, वायरल संक्रमण, हैजा, तंत्रिका संबंधी विकार, प्रजनन संबंधी समस्याएं और पौधों में फंगल रोग शामिल हैं। परिसर में डिलीवरी सिस्टम विकसित करने, बीमारी के दौरान सेलुलर फ़ंक्शन के मूल सिद्धांतों को समझने और रोग अभिव्यक्तियों के आणविक वर्गीकरण को चिह्नित करने के लिए उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण, डीएनए बार-कोडिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, नैनो-बायोटेक्नोलॉजी और रासायनिक जीव विज्ञान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मुख्य परिसर से लगभग 10 किमी दूर अक्कुलम में स्थित दूसरा परिसर, टीकों और प्रतिरक्षा-चिकित्सा, आणविक निदान, बायोमार्कर, रासायनिक और नैनो-जैव प्रौद्योगिकी और उष्णकटिबंधीय रोग जीव विज्ञान पर शोध का केंद्र है। यह गहरे और उन्नत स्तर के तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित मध्यम और उच्च-स्तरीय नवाचार के लिए एक अनूठा ज्ञान केंद्र है। बायो-इमेजिंग, जीनोमिक्स और प्रयोगशाला चिकित्सा, आणविक निदान और रासायनिक जीव विज्ञान, रोगज़नक़ जीव विज्ञान, कैंसर अनुसंधान और कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान के लिए कुछ प्रयोगशालाएँ इस परिसर में हैं। तीसरी सुविधा, बायोनेस्ट, केरल के औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र, कोच्चि में कलामस्सेरी में केरल प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में केरल स्टार्ट-अप मिशन के सहयोग से आर जी सी बी द्वारा संचालित की जाती है। बायोनेस्ट परिसर स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों (एसएमई), शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के लिए एक ऊष्मायन केंद्र है। यह नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म और इनक्यूबेटर सुविधाएं प्रदान करता है। बायोनेस्ट का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाना, उभरते उद्यमों का पोषण करना और अन्य जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों, शिक्षाविदों और सरकार के साथ उचित संबंध बनाने में नए उद्यमों की सहायता करना है। बायोनेस्ट एमएससी/बी.टेक/एम.टेक बायोटेक छात्रों को उनके शोध प्रबंध और परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए अल्पकालिक औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सुविधाएं भी प्रदान करता है।
इस प्रकार आर जी सी बी जैव प्रौद्योगिकी को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अब तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे क्षितिज स्पष्ट हैं और रास्ते अच्छी तरह से परिभाषित हैं। हम भारत को जैव प्रौद्योगिकी में एक ज्ञान शक्ति बनाने में योगदान देने के अपने कार्य को पूरा करेंगे। केरल राज्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भी अधिक समर्पण के साथ जारी है। न्यायपालिका और आपराधिक न्याय प्रणाली को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए बारकोडिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा, आर जी सी बी वायरल रोगों, कैंसर मार्करों और हृदय और आनुवंशिक रोगों के लिए जोखिम मार्करों के लिए अत्याधुनिक आणविक निदान प्रदान करता है।
इस प्रकार आर जी सी बी भारतीय जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान के भविष्य को प्रतिबिंबित करेगा
राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आर जी सी बी) की शुरुआत 03 जुलाई, 1990 को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सी-डेस्ट) के रूप में हुई थी, जो एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसे त्रावणकोर कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1955 (पंजीकरण संख्या 418/90) के तहत प्रसिद्ध पेशेवरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा अनुसंधान, क्षेत्र अध्ययन, कार्रवाई परियोजनाओं आदि को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने सी-डेस्ट सोसायटी के मुख्य संरक्षक बनने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह हमारे लिए गर्व की बात थी कि श्री के.आर. नारायणन, जो पहले शासी निकाय के सदस्यों में से एक थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। संस्थान के प्रथम शासी निकाय के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों में शामिल थे, श्री जी. कार्तिकेयन [शासी निकाय के अध्यक्ष और केरल विधान सभा के सदस्य], श्री पंडालम सुधाकरण, [पूर्व मंत्री, केरल सरकार], श्री आर. रामचंद्रन नायर, आई ए एस, [पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, केरल सरकार<], डॉ. वी.के. सुकुमारन नायर [पूर्व कुलपति, केरल विश्वविद्यालय],डॉ. टी. नवनीत राव, [पूर्व कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय], डॉ. (सुश्री) डी. बंगाली [पूर्व कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय], डॉ. टी.के. रवींद्रन [पूर्व कुलपति, कालीकट विश्वविद्यालय],डॉ. एम. एल. मेहता [पूर्व अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली], डॉ. वी.आई. सुब्रमण्यम, [पूर्व कुलपति & निदेशक, इंटरनेशनल स्कूल द्रविड़ियन भाषाविज्ञान, तिरुवनंतपुरम], प्रोफेसर निनान अब्राहम[पूर्व कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय], डॉ. ए.टी. देवासिया [पूर्व कुलपति, गांधीजी विश्वविद्यालय], डॉ. (सुश्री) जे.के. पिल्लई [पूर्व कुलपति, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, मद्रास], प्रोफेसर मुहरजिरी [वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय, बारबाडोस, वेस्ट इंडीज], डॉ. सी. एन. पुरुषोत्तमन नायर [पूर्व प्रोफेसर & प्रमुख, वाणिज्य विभाग, & डीन, वाणिज्य संकाय, केरल विश्वविद्यालय], डॉ. के.ए.एल. नारायण स्वामी [जनरल मैनेजर, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, तिरुवनंतपुरम],डॉ. रॉय वर्गीस [पूर्व प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम], और श्री अदूर प्रकाश [कानूनी विशेषज्ञ, अदूर]। डॉ. ए. सुकुमारन नायर सी-डेस्ट के निदेशक थे और डॉ. आर. अशोक इसके रजिस्ट्रार थे।
संस्थान के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उसे वर्ष 1990 में देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के ग्रेडिंग मानकों की जिम्मेदारी दी गई थी, एक मान्यता प्रणाली जिसे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएचई) के माध्यम से प्रशासित किया जाना था।
इसके बाद संस्थान का नाम बदलकर राजीव गांधी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (आरजीसी-डीईएसटी) कर दिया गया, जो श्री राजीव गांधी के दुखद निधन के बाद उनके नाम पर रखा जाने वाला देश का पहला संस्थान बन गया। इसके बाद 16 अक्टूबर, 1991 को यह केरल सरकार का "अनुदान-सहायता" संस्थान बन गया। राज्य के लिए राजीव गांधी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की सेवाओं की क्षमता और उपयोगिता को समझते हुए, केरल सरकार ने संस्थान को स्थापना अनुदान के रूप में महत्वपूर्ण कोर सहायता प्रदान की। केरल सरकार ने 12 मार्च, 1993 के सरकारी आदेश के अनुसार राजीव गांधी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के शासी निकाय और कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया, ताकि केंद्र के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण हो सके और इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पर राज्य समिति (एसटीईसी) के अधीन लाया जा सके। पुनर्गठित शासी निकाय के गठन में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया और डॉ. ए. सुकुमारन नायर, डॉ. रॉय वर्गीस, डॉ. वी.के. सुकुमारन नायर, श्री के.ए.एल. नारायणस्वामी, डॉ. सी.एन. पुरुषोत्तमन नायर, शासी निकाय द्वारा नामित सात शिक्षाविद/पेशेवर और सरकार के निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल थे: श्री आर. रामचंद्रन नायर, [आयुक्त एवं सचिव वन], श्री एम. मोहन कुमार, [आयुक्त एवं वित्त सचिव], श्री के.वी. नांबियार, [योजना सचिव], डॉ. आर. रविकुमार [विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव], श्री सी.वी. आनंद बोस, [निर्मिति केंद्र के निदेशक] और श्री के.के. विजयकुमार [सामान्य शिक्षा सचिव] तथा स्टाफ प्रतिनिधि के रूप में श्री एस. मोहनन नायर, कार्यक्रम अधिकारी, राजीव गांधी विकास, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। डॉ. एन. ऋषि, पूर्व निदेशक, सीटीसीआरआई और सलाहकार एफएओ, संयुक्त राष्ट्र को एसटीईसी के तहत अनुदान सहायता संस्थान बनने के बाद संस्थान के प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
इसके बाद केरल सरकार ने संस्थान को केरल राज्य का पूर्ण विकसित अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के सदस्यों में डॉ. पी.के. अयंगर, [परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और केरल सरकार के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार, केरल सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (एसटीईसी) पर राज्य समिति के तत्कालीन अध्यक्ष], श्री वी. रामचंद्रन, आईएएस, [राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष], डॉ. एम.एस. वलियाथन, [मणिपाल विश्वविद्यालय के कुलपति] और श्री के.वी. नांबियार, आईएएस [योजना आयोग के सदस्य] शामिल थे।
विशेषज्ञ आयोग ने आर जी सी-डीईएसटी के पुनर्गठन के सभी पहलुओं की जांच की और केरल सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी, ताकि जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्रों के लिए समर्पित एक संस्थान शुरू किया जा सके। केरल सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और संस्थान का पुनर्गठन करने और इसे आवश्यक अतिरिक्त इनपुट के साथ एसटीईसी के तहत जैव प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में उन्नत करने का संकल्प लिया। केरल सरकार ने संस्थान को एक व्यापक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में पुनर्गठित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और इस प्रकार 18 अप्रैल, 1994 को राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी) की स्थापना की गई। आरजीसीबी भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए स्थापित पहला शोध संस्थान था। ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉ. पी. पुष्पांगदन को आर जी सी बी के निदेशक का प्रभार दिया गया। डॉ. एम.आर. दास, भारत के बेहतरीन आणविक जीवविज्ञानी को खोज समिति की सिफारिशों के अनुसार आर जी सी बी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

राजीव गांधी (20 अगस्त, 1944 से 21 मई, 1991) 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और नई उभरती भारतीय पीढ़ी के प्रतीक थे - साहसी, नवोन्मेषी और ऊर्जा से भरपूर। उन्होंने यह भी साबित किया कि परंपरा निरंतर और गहरी होती है। अपने दादा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह, राजीव गांधी का दृढ़ विश्वास था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही वह आधारशिला है जिस पर भारत की नियति के साथ मुलाकात फलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास ने राजीव गांधी के प्रिय वाक्यांश "मेरा भारत महान" के लिए भी रीढ़ प्रदान की। भारत की संपत्तियों में हमेशा संभावना देखने वाले, उन्होंने भारत की बौद्धिक जनशक्ति को विदेशों में निर्यात करने को ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि एक ब्रेन बैंक कहा, जिस पर जरूरत और अवसर के समय भरोसा किया जा सकता है। आज भारत एक आईटी दिग्गज के रूप में अपनी स्थिति बना पाया है, जिसका श्रेय राजीव गांधी द्वारा कम्प्यूटरीकरण पर लिए गए पथ-प्रदर्शक निर्णयों को जाता है। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की और प्रौद्योगिकी विकास की देखरेख के लिए पांच महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की - जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान और महासागर विकास। इन महत्वपूर्ण रचनाओं के परिणाम आज सभी के सामने हैं।
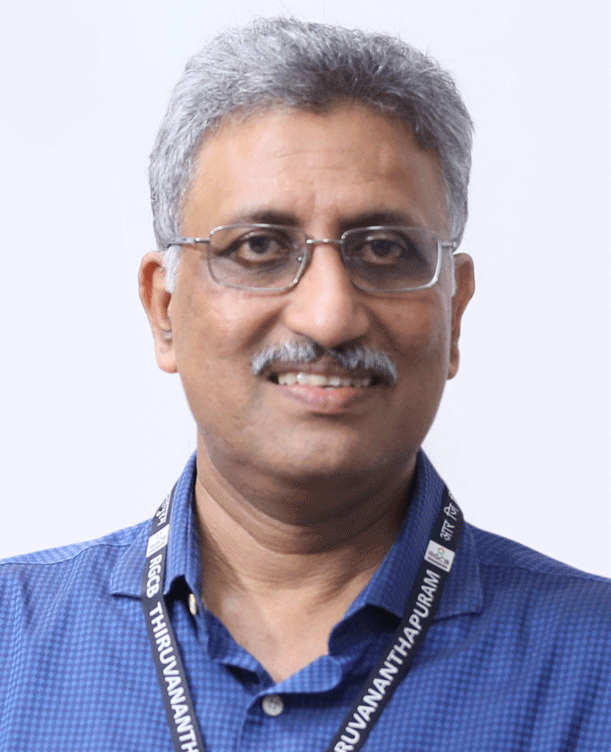
निदेशक
राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र 06 नवंबर, 2020 से अब तक
प्रोफेसर चंद्रभास नारायण 06 नवंबर, 2020 को निदेशक के रूप में आरजीसीबी में शामिल हुए। प्रो. नारायण जन्म से बैंगलोर के निवासी हैं, उनके माता-पिता केरल से हैं। उन्होंने मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (मैसूर विश्वविद्यालय से संबद्ध) से विज्ञान शिक्षा में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के भौतिकी विभाग से पीएचडी की। वे अपने पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इथाका, न्यूयॉर्क गए। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी) में निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले, वे जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर) में डीन (अनुसंधान और विकास), अध्यक्ष (रसायन विज्ञान और भौतिकी) और डीन (फेलोशिप और विस्तार कार्यक्रम) थे। प्रो. नारायण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विशेषज्ञ हैं। एक प्रशिक्षित संघनित पदार्थ भौतिक विज्ञानी होने के बावजूद, प्रो. नारायण ने जेएनसीएएसआर में कुछ ही वर्षों में जीव विज्ञान में गहरी रुचि विकसित कर ली। उनका समूह ए) ड्रग-प्रोटीन इंटरैक्शन, ड्रग स्क्रीनिंग अनुप्रयोगों, बी) प्रोटीन संरचना कार्य अध्ययन और सी) डायग्नोस्टिक अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग में अग्रणी है। इन क्षेत्रों में उनके कई कार्य अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान में ट्रेंडसेटर हैं। जीवविज्ञान में उनकी रुचि के साथ-साथ, वे भौतिकी और रसायन विज्ञान में भी अपनी रुचि रखते हैं। कुल मिलाकर उनका समूह भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान के क्षेत्रों में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग के लिए देश के प्रसिद्ध समूहों में से एक रहा है। इस प्रक्रिया में, उनके पास तीन अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं, जिनमें से कुछ व्यावसायीकरण के कगार पर हैं। वे हाल ही में भारत के लिए दो प्रमुख सिंक्रोट्रॉन परियोजनाओं के समन्वयक थे, अर्थात्, फोटॉन फैक्ट्री में भारतीय बीमलाइन, केईके, त्सुकुबा, जापान और पेट्रा III, हैम्बर्ग, जर्मनी। यह कार्यक्रम भारत में शोधकर्ताओं को सिंक्रोट्रॉन का उपयोग करके विभिन्न प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। जेएनसीएएसआर में उनकी लाइट स्कैटरिंग प्रयोगशाला रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ब्रिलौइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उच्च दबाव और तापमान के तहत एक्स-रे विवर्तन का उपयोग करके सामग्री के भौतिक गुणों को देखने में रुचि रखती है। शोध समस्याओं में संघनित पदार्थ, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल हैं। उन्हें 2007 में मैटेरियल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक, 2008 में सर सी.वी. रमन यंग वैज्ञानिक पुरस्कार (कर्नाटक सरकार), 2008 में सी.एन.आर. राव ओरेशन अवार्ड 2009 में, शेख सकर RAK-CAM सीनियर फेलो 2016 में, MRSI-ICSC सुपर कंडक्टिविटी और मैटेरियल साइंस सीनियर अवार्ड 2017 में, मिजुशिमा-रमन लेक्चर अवार्ड 2018 में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्लेटिनम जुबली लेक्चर अवार्ड 2020 में, उनके शोध योगदान के लिए। वे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, भारत के फेलो, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के फेलो हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 180 से अधिक शोध पत्र और पुस्तकों में 4 अध्याय प्रकाशित किए हैं और उनका एच-इंडेक्स 39 है। उनके प्रकाशनों में नेचर, एडवांस्ड मैटेरियल्स, एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (यूएसए), फिजिकल रिव्यू लेटर्स, एंजवेन्टे केमी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिकल रिव्यू बी, जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लेटर्स, आदि शामिल हैं। इससे उनके शोध की अंतःविषय प्रकृति का पता चलता है, जो वर्तमान स्थिति में हर शोध के लिए जरूरी है। वे 2001 से 2007 तक कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इथाका, न्यूयॉर्क, यूएसए में विजिटिंग प्रोफेसर थे और 2008 से 2016 तक इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरलॉजी एंड फिजिक्स ऑफ डेंस मैटर, यूनिवर्सिटी ऑफ पियरे एंड मैरी क्यूरी, पेरिस, फ्रांस में विजिटिंग प्रोफेसर थे। वे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के संपादकों में से एक हैं: जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजिक्स (अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स), हाई-प्रेशर रिसर्च (टेलर एंड फ्रांसिस पब्लिशर्स), जर्नल ऑफ बायोमटेरियल्स एंड नैनोबायोटेक्नोलॉजी। वे रेवा यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के कॉर्पोरेट सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, बेंगलुरु के शासी निकाय के सदस्य हैं और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के रसायन विज्ञान विभाग, एम.एस. रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भौतिकी विभाग, रेवा विश्वविद्यालय और कालीकट विश्वविद्यालय में नैनोटेक्नोलॉजी विभाग के अध्ययन बोर्ड के सदस्य थे।

[ मार्च 01, 2005 से अगस्त 20, 2020 ]
प्रोफेसर एम. राधाकृष्ण पिल्लई 1 मार्च, 2005 को आर जी सी बी में शामिल हुए, क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में आणविक चिकित्सा के प्रोफेसर के रूप में एक सफल कैरियर के बाद, वे 44 वर्ष की उम्र में एक राष्ट्रीय शोध संस्थान के सबसे कम उम्र के प्रमुख बन गए। रोग जीव विज्ञान और नैदानिक जैव प्रौद्योगिकी में 31 से अधिक वर्षों के पोस्टडॉक्टरल शोध अनुभव वाले एक वैज्ञानिक, वे रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट (लंदन), तीनों भारतीय विज्ञान अकादमियों और भारतीय चिकित्सा अकादमी के एक निर्वाचित फेलो हैं।
1,341 / 5,000 आर जी सी बी 2005 में एक राज्य सरकार का संस्थान था, जिसका प्रदर्शन सूचकांक सामान्य था और बुनियादी ढांचा सीमित था। एक दूरदर्शी व्यक्ति तब खुद को अलग पहचान देता है जब वह दूसरों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसर खोज लेता है। जब प्रोफेसर पिल्लई ने आरजीसीबी में कार्यभार संभाला तो बुनियादी ढांचे, कर्मियों और धन की कमी के कारण उनका स्वागत किया गया। लेकिन उन्होंने इसे संभावनाओं की खोज, कल्पना और उत्कृष्ट विचारों को क्रियान्वित करने की एक धन्य स्वतंत्रता के रूप में पाया। यह उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति और दिशा ही थी जिसके कारण भारत सरकार ने 2007 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में आरजीसीबी को अपने अधीन कर लिया। परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। आरजीसीबी आज एक महत्वपूर्ण स्थान वाला केंद्र है, जो अपने विशिष्ट रोग जीवविज्ञान कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, जिसमें अंतःविषय विज्ञान का उपयोग रोग रोगजनन में प्रासंगिक प्रश्न पूछने के लिए प्रभावी रूप से किया जाता है। कोशिका जीवविज्ञानियों को रोगविज्ञानियों, बहुलक रसायनज्ञों और यहां तक कि पादप जीवविज्ञानियों के साथ मिलकर पुरानी और संक्रामक बीमारियों में व्यवहार्य सफल कार्यक्रम विकसित करना आर जी सी बी की एक उल्लेखनीय विशेषता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशनों और पेटेंटों की मात्रा और गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त वृद्धि हुई है।
प्रोफेसर पिल्लई ने एक अद्वितीय जैव-नवप्रवर्तन केंद्र (बीआईसी) बनाने के लिए आर जी सी बी के दूसरे चरण के विकास का भी सफलतापूर्वक संचालन किया। आर जी सी बी में अब तक मुख्य रूप से अन्वेषक संचालित विज्ञान पर जोर दिया गया था, जबकि दूसरे चरण में त्वरित खोज और शीघ्र अनुवाद के लिए टीम संचालित विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस नए नवाचार केंद्र की अवधारणा वर्तमान संस्थान के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ने के लिए की गई है, जो खोज विज्ञान और अनुवाद के लिए एक उत्कृष्ट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। 100 करोड़ रुपये की यह परियोजना वर्तमान में अपने अंतिम चरण में है। प्रोफेसर पिल्लई ने राज्य सरकार को इस परियोजना के लिए शहर के मध्य में 20 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के लिए राजी किया, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि भारतीय वायु सेना और अंतरिक्ष विभाग को भी भूमि के लिए भुगतान करना पड़ा। आर जी सी बी गवर्निंग काउंसिल ने उच्च नियंत्रण सुविधाओं सहित वायरल रोग जीवविज्ञान और वैक्सीन विकास के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान के लिए 430 करोड़ रुपये की मास्टर प्लान को भी अनंतिम रूप से मंजूरी दे दी है।
प्रोफेसर पिल्लई ने कोच्चि में एक प्रौद्योगिकी विकास इनक्यूबेटर - बायोनेस्ट का प्रबंधन करके नए स्टार्ट अप उद्योगों और शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षण सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के उपयोग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए आरजीसीबी की उत्कृष्ट विशेषज्ञता का उपयोग किया। राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित, बायोनेस्ट, एक बायो-इनक्यूबेटर सुविधा नई प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने, उभरते उद्यमों को पोषित करने और नए उद्यमों को अन्य बायोटेक कंपनियों, शिक्षाविदों और सरकार के साथ उचित संबंध बनाने में सहायता करने का काम करती है। बायोनेस्ट का उद्देश्य आने वाली बायोटेक/फार्मा कंपनियों को नई प्रौद्योगिकियों के लाइसेंस के लिए एक व्यवहार्य तंत्र प्रदान करना, नए स्थानीय उद्यम शुरू करना और न्यूनतम वित्तीय इनपुट के साथ प्रौद्योगिकी का प्रारंभिक राज्य मूल्य संवर्धन प्राप्त करना है। बायोनेस्ट के डिलीवरेबल्स में प्रौद्योगिकी पैकेज, नए उत्पाद पोर्टफोलियो, नए उत्पादों के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और परियोजना रिपोर्ट, प्रक्रिया/उत्पाद पेटेंट, नए उपकरणों के प्रोटोटाइप और समृद्ध प्रबंधन अनुभव शामिल हैं। बायोनेस्ट, जिसमें पहले से ही 26 कंपनियाँ शामिल हैं, प्रौद्योगिकी विकास, स्केल-अप और ट्रांसलेशनल बायोटेक्नोलॉजी में नई नौकरियों का सृजन भी करेगा।
हमेशा वैज्ञानिक उपलब्धियाँ ही किसी वैज्ञानिक को महान नहीं बनातीं, बल्कि वह सबसे छोटी उपलब्धियों को भी मानवता की सेवा के लिए प्रभावी साधन में बदल देता है। 2006 से 2011 की अवधि के दौरान, केरल में चिकनगुनिया और डेंगू सहित वायरल बुखार के बहुत गंभीर प्रकोप थे, जिसके बाद H1N1 फ्लू महामारी फैल गई। राज्य में आणविक वायरल निदान करने के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं थी और केरल की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की सहायता के लिए RGCB की विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए प्रोफेसर पिल्लई की ओर रुख किया। अपनी प्रतिबद्धता और चरित्र के अनुरूप, प्रोफेसर पिल्लई ने प्रयोगशाला चिकित्सा और आणविक निदान (LMMD) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहन की स्थापना की। LMMD जिसने 3 वायरल डायग्नोस्टिक्स के साथ शुरुआत की, अब 40 से अधिक वायरल और बैक्टीरियल मापदंडों का प्रदर्शन करता है और वर्तमान में यह भारत में एकमात्र ऐसी सुविधा है जो एक ही छत के नीचे इतने सारे मापदंडों का प्रदर्शन करती है। इन सेवाओं की मान्यता में ही भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने इस प्रयोगशाला को राष्ट्रीय वायरोलॉजी नेटवर्क ग्रेड 1 प्रयोगशाला के रूप में नामित किया। आगे की मान्यता तब मिली जब सुविधा को NABL और NABH दोनों द्वारा मान्यता दी गई। कोविड 19 महामारी के आगमन के साथ, यह स्वाभाविक ही था कि RGCB कोविड 19 डायग्नोस्टिक्स और नए डायग्नोस्टिक किट के लिए एक स्वीकृत मान्यता प्राप्त सत्यापन केंद्र दोनों के लिए एक अग्रणी बन गया। इन उपलब्धियों को और बढ़ाने के लिए, बड़े वैक्सीन क्षेत्र परीक्षणों में अपने अनुभव के साथ, प्रोफेसर पिल्लई ने RGCB को मेयो क्लिनिक और बायोटेक कंपनी टेथरेक्स के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया, जो जल्द ही भारत में एक नए उम्मीदवार वैक्सीन परीक्षण की शुरुआत करेगी, जहाँ सभी प्रतिरक्षा मापदंडों को RGCB में किया जाएगा। फिर से यह किसी भी शोध संस्थान के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी।
प्रोफेसर पिल्लई के नेतृत्व में, आर जी सी बी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेवाओं के लिए राज्य सरकार को अपना मजबूत समर्थन जारी रखा। केरल राज्य में आई दो बड़ी त्रासदियों के मद्देनजर इन सेवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। कोल्लम में हुई भीषण आतिशबाजी त्रासदी और ओची चक्रवात के कारण बड़ी संख्या में अज्ञात शवों की पहचान की जानी थी और उन्हें उनके परिजनों को लौटाना पड़ा। छोटी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुविधा जिसे एक पूर्ण विकसित आणविक फोरेंसिक प्रयोगशाला में अपग्रेड किया गया था, ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजे गए सैकड़ों शवों की पहचान करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम किया। इस विशाल सामाजिक सेवा ने आरजीसीबी को जबरदस्त सार्वजनिक सद्भावना और प्रशंसा अर्जित की है। यह प्रयोगशाला अब एनएबीएल और एनएबीएच दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और मानव डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वन्यजीव फोरेंसिक के लिए डीएनए बारकोडिंग और पूरे भारत में जीवविज्ञानियों के लिए अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बारकोडिंग आधारित शोध परियोजनाओं को आउटसोर्स करने के लिए एक शोध सुविधा प्रदान करती है। इन उपलब्धियों के परिणामस्वरूप, आरजीसीबी अब भारत मानव जीनोम कार्यक्रम में एक वरिष्ठ भागीदार भी है जिसका उद्देश्य भारत की आबादी के विभिन्न वर्गों के डीएनए फिंगरप्रिंट लेना है। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप, उन्होंने राज्य में आई बाढ़ में बाढ़ राहत उपायों के लिए संस्थान की प्रयोगशालाएँ खोलीं। इसमें बाढ़ के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से निपटने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करना और राज्य में विभिन्न चिकित्सा शिविरों में वितरित किए जाने वाले धन और सामग्री की व्यवस्था करना शामिल है।
अध्यापन हमेशा से प्रोफेसर पिल्लई का प्राथमिक जुनून रहा है। उन्होंने सफलतापूर्वक आर जी सी बी के पीएचडी कार्यक्रम को देश में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिस्पर्धी में से एक बनाया और साथ ही भारत का पहला अनन्य पीएचडी इन ट्रांसलेशनल साइंस एंड मेडिसिन (टीएसएम) कार्यक्रम भी शुरू किया, जो चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान और फार्मेसी में टर्मिनल डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वे ट्रांसलेशनल साइंस की अगली पीढ़ी के नेता बन सकें। प्रोफेसर पिल्लई के मार्गदर्शन में सत्ताईस भाग्यशाली छात्रों ने पीएचडी की। एक और उल्लेखनीय घटना आरजीसीबी में बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर प्रोग्राम की शुरुआत थी, जिसमें रोग जीव विज्ञान, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और आणविक निदान में अद्वितीय विशेषज्ञता थी। यह कार्यक्रम भारत में सबसे अच्छे और सबसे अधिक मांग वाले कार्यक्रमों में से एक बन गया है।
आर जी सी बी में प्रोफेसर एम राधाकृष्ण पिल्लई ने वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में एक अद्वितीय ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मार्ग प्रशस्त किया और विज्ञान को प्रयोगशालाओं से सीधे सार्वजनिक लाभ तक ले जाने का एक आदर्श उदाहरण है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर पर उनका काम है, जो भारत में महिलाओं में सबसे अधिक बार होने वाला कैंसर है, जो मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होता है। वर्तमान अनुमान बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 132,000 नए मामलों का निदान किया जाता है और 74,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 1/3 हिस्सा है। प्रोफेसर पिल्लई ने वायरस की जटिल विकृति पर विशाल ज्ञान का उत्पादन किया; उन्होंने आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव रसायन और महामारी विज्ञान में अपने सभी संसाधनों को एचपीवी संक्रमण के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने के लिए लगाया। इसे पहचानते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय महिलाओं में एचपीवी के खिलाफ 3-खुराक वाले टीके के भारी आर्थिक और सामाजिक बोझ को कम करने के लिए प्रोफेसर पिल्लई का समर्थन किया। इन अध्ययनों ने तर्कसंगत रूप से 2-खुराक वाले टीके की प्रभावकारिता को साबित किया, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है। उन्होंने यह भी साबित किया कि वैक्सीन की एक खुराक में संक्रमण को रोकने की महत्वपूर्ण क्षमता भी है। प्रतिष्ठित लैंसेट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमानों को बदल दिया। पत्रिका ने एक टिप्पणी में लिखा है कि "यह अध्ययन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के उच्च बोझ वाले देशों में संक्रमण और बीमारी को रोकने में एचपीवी टीकों की भूमिका को समझने में दीर्घकालिक योगदान देगा। इस वैक्सीन अध्ययन में भाग लेने वाली भारतीय महिलाओं का अनुभव औपचारिक यादृच्छिक परीक्षणों की स्थापना के दौरान एक-खुराक एचपीवी टीकाकरण के मूल्यांकन में अग्रणी होने का वादा करता है"।
प्रोफेसर पिल्लई ने हमेशा संस्थान के वैज्ञानिकों को अनुसंधान के वित्तपोषण में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया और वित्तपोषण के लिए संस्थान पर न्यूनतम निर्भरता रखी। उन्होंने अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने में असाधारण प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के माध्यम से आरजीसीबी में इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मानक स्थापित किए। उन्हें कैंसर के खिलाफ अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (डब्ल्यूएचओ) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (₹25 करोड़), खसरा वैक्सीन विफलता पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, यूएसए द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम (₹4 करोड़), जैव प्रौद्योगिकी विभाग से ट्रांसलेशनल ब्रेस्ट कैंसर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र (₹4 करोड़), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से राष्ट्रीय औषधि डिजाइन केंद्र (₹4 करोड़), क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के साथ ट्रांसलेशनल कैंसर अनुसंधान के लिए एक अनूठा "ग्लू अनुदान" (₹4 करोड़), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से आदिवासी प्रौद्योगिकी के अनुवाद के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र (₹4 करोड़) - इसके अलावा ₹40 से 90 लाख तक के कई छोटे अनुदान प्राप्त हुए हैं। 220 से अधिक सहकर्मी-समीक्षित प्रकाशनों और 42 के एच इंडेक्स के साथ, प्रोफेसर पिल्लई अपने अग्रणी शोध में खुद को पूरी तरह से व्यस्त रखते हुए देश में वर्तमान शोध उद्यम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यह एक वैज्ञानिक अनुचर के साथ-साथ संस्थान कमांडर के रूप में उनकी सफलता का मुख्य कारण था, साथ ही 15 वर्षों के निरंतर कार्यकाल के लिए एक राष्ट्रीय शोध संस्थान का नेतृत्व करने का अनूठा सम्मान भी मिला।
प्रोफेसर पिल्लई ने प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को भी प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित किया और आज आर जी सी बी एक अत्यंत कुशल संस्था है। प्रशासक के रूप में उनकी उपलब्धियों में से एक यह तथ्य है कि आर जी सी बी के पास आज देश की सबसे अच्छी सामाजिक कल्याण योजनाएँ हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एकमात्र संस्थान है जिसने 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा में अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की पुरानी पेंशन योजना के बराबर एक व्यापक पेंशन योजना बनाई है। यह एलआईसी को संस्थान के स्व-निर्मित फंड को नैदानिक निदान, सेवाओं और परामर्श के साथ-साथ ईपीएफ योगदान से प्रबंधित करने के लिए कहकर किया गया था, जिससे भारत सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा। आर जी सी बी अपने कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल सुविधाओं में से एक का दावा करता है, जिसमें सरकारी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में "नकद रहित" पहुँच शामिल है।
प्रोफेसर एम. राधाकृष्ण पिल्लई, जो 31 अगस्त, 2020 को आर जी सी बी से सेवानिवृत्त हुए, निस्संदेह भारत के सबसे प्रसिद्ध शोधकर्ताओं में से एक हैं और एक असाधारण व्यक्ति हैं जो मानवता की भलाई के लिए ज्ञान की तलाश करते हैं। आरजीसीबी वास्तव में इस नेता का ऋणी है, जिसने संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बना दिया है।

[ दिसंबर 2001 से 28 फरवरी 2005 तक ]
राघव वर्मन थम्पन ने 1968 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से प्राणीशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने सेल बायोलॉजी विभाग, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए और मॉलिक्यूलर बायोफिज़िक्स यूनिट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर में पोस्टडॉक्टरल प्रशिक्षण प्राप्त किया।
डॉ. थम्पन की शोध रुचियों का मुख्य ध्यान एस्ट्रोजन क्रिया में आणविक तंत्रों के शोध पर था, जिसमें दो प्रोटीनों, गैर-सक्रिय एस्ट्रोजन रिसेप्टर (naER) और एस्ट्रोजन रिसेप्टर सक्रियण कारक (ERAF) के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया था। उनकी प्रमुख खोजों में से एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर α (ER α) के परमाणु प्रवेश में शामिल परमाणु परिवहन प्रोटीन की पहचान, अलगाव और लक्षण वर्णन था। इन अध्ययनों के विस्तार ने परिवहन में एस्ट्राडियोल की भूमिका को और उजागर किया, जिसमें प्रोटीन p28 और p73 की भागीदारी थी। उनका शोध समूह यह प्रदर्शित करने वाला पहला था कि ER α का क्षरण एस्ट्राडियोल पर निर्भर ER α के यूबिक्विटिनेशन द्वारा मध्यस्थता करता है। इस समूह के श्रेय में एक और 'पहला' प्लाज्मा झिल्ली स्थानीयकृत एस्ट्रोजन रिसेप्टर, naER का शुद्धिकरण है, जो टायरोसिन किनेज के रूप में कार्य करने वाला पहला स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर है। इन अध्ययनों के दौरान यह देखा गया कि ग्लाइकोप्रोटीन, naER, नाभिक में चला जाता है और डीग्लाइकोसिलेटेड होकर परमाणु एस्ट्रोजन रिसेप्टर II (nER II) में परिवर्तित हो जाता है, जो जाहिर तौर पर मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन (m RNP) के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक परिवहन में प्रमुख कार्यात्मक भूमिका निभाता है।
डॉ. थम्पन के कार्यकाल के दौरान आरजीसीबी ने अपने संकाय की संख्या में वृद्धि की और अपने बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किया। छात्र आवासों सहित वर्तमान मुख्य परिसर का अधिकांश निर्माण निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ।

[ अगस्त 1994 से दिसंबर 2001 ]
यह भारत के बेहतरीन आणविक जीवविज्ञानियों में से एक मुक्कट्टू रामचंद्र दास की दूरदर्शिता, दूरदर्शिता और अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि जैव प्रौद्योगिकी को राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आर जी सी बी) के अधिदेश के रूप में लाया गया। केरल सरकार और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से उन्होंने संस्थान को आधुनिक और अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया। एम.आर.दास ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण समिति (एसटीईसी) के अध्यक्ष और केरल सरकार के पदेन प्रधान सचिव का पद भी संभाला। उन्होंने एसटीईसी के तहत सात विज्ञान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे और अनुसंधान विकास गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रामचंद्र दास का जन्म 2 जुलाई 1937 को केरल के तिरुवल्ला में हुआ था। युवा रामचंद्र ऐसे माहौल में पले-बढ़े, जिसने रचनात्मक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया और स्कूल में ही उनमें गणित और विज्ञान के प्रति प्रेम और साहित्य और ललित कलाओं में गहरी रुचि विकसित हो गई। केरल विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एम.एस.सी. की डिग्री पूरी करने के बाद, योग्यता क्रम में प्रथम स्थान पर, एम.आर. दास, सिविल सेवा में करियर के बजाय विज्ञान को प्राथमिकता देते हुए, पीएचडी के लिए शोध सहायक के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टी.आई.एफ.आर.), बॉम्बे में शामिल हो गए। उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन के सबसे प्रभावशाली और उत्पादक 36 वर्ष केरल के बाहर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टी.आई.एफ.आर.), मुंबई, कोलंबिया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, मिशिगन कैंसर फाउंडेशन, डेट्रायट और फिर सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, (सी.सी.एम.बी.), हैदराबाद में बिताए।
1958 से 1969 की अवधि के दौरान, दास के शोध कार्य में इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस (ESR) और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डबल रेजोनेंस (ENDOR) जैसे चुंबकीय अनुनाद विधियों का उपयोग करके कुनैन जैसे कुछ जैविक रूप से दिलचस्प अणुओं में अंतःक्रियाओं की ज्यामिति, संरचना और तंत्र को समझने के अध्ययन शामिल थे। दास का सबसे प्रसिद्ध कार्य, 1969 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सोल स्पीगलमैन के साथ मिलकर, एवियन और म्यूरिन मूल के ट्यूमर वायरल आरएनए और उनके मेजबान डीएनए के बीच न्यूक्लिक एसिड समरूपता के स्पष्ट प्रदर्शन से संबंधित था। यह रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस की खोज से पहले हुआ था। ये अध्ययन 1970 में नेचर के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंकों में तीन पत्रों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुए थे।
दास भारत में सभी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के निर्वाचित फेलो थे। उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें बुनियादी चिकित्सा विज्ञान में शोध के लिए हरिओम आश्रम पुरस्कार, कैंसर अनुसंधान के लिए आईसीएमआर का सैंडोज़ ओरेशन पुरस्कार और चिकित्सा विज्ञान के लिए रैनबैक्सी पुरस्कार शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2003 को उनकी अचानक मृत्यु के समय वे भारत में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर थे।